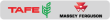बांग्लादेश के नौका स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे (Courtesy: SSS)
Floating School in Bangladesh: भारत की तरह बांग्लादेश भी नदियों का देश है। बांग्लादेश भी बाढ़ की समस्या से हर साल दो-चार होता रहता है। बाढ़ की चपेट में आने पर सड़क और गांव से स्कूल तक पहुंचना मुश्किल या असंभव सा हो जाता है। ऐसे में बांग्लादेश के एक शख्स ने पानी में तैरती हुई नौका पर पूरा स्कूल बना दिया और एक नई इबारत लिख डाली।
इस स्कूल के संस्थापक और येल विश्वविद्यालय के फेलो रिजवान का कहना है कि सौर ऊर्जा से संचालित "तैरते स्कूल" यह तय करते हैं कि बाढ़ के बावजूद भी बच्चों के हाथों से किताब नहीं छूटे। भारत में भी बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए तरह-तरह के व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गिजुभाई बधेका के प्रयास सराहनीय हैं। भारत में कई जगहों पर पटरी वाले स्कूल, फ्लाईओवर के नीचे सायंकालीन स्कूल चलाए जाते हैं।
मोहम्मद रिजवान ने शिधुलाई स्वनिर्वर संस्था (Shidhulai Swanirvar Sangstha) बनाई और वर्ष 2002 में दुनिया के सामने पहली तैरती हुई स्कूल अवधारणा को लागू किया। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति की राशि के 500 डॉलर रुपये से से फ्लोटिंग स्कूल की शुरूआत की थी। ये स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चालित हैं। मोहम्मद रिजवान पेशे से आर्किटेक्ट हैं।
पश्चिमी बांग्लादेश के इस स्कूल में पढ़ने वाले 2240 छात्र हर सुबह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर नौका वाली स्कूल का इंतजार करते हैं। स्कूल उनके दरवाजे तक आकर उन्हें पठन-पाठन की दुनिया में ले जाता है। बांग्लादेश के चालन बील क्षेत्र में 100 नावें कक्षाओं के रूप में काम करती हैं। इन स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई हैं। ये स्कूल नदी किनारे के गांवों का दौरा करती हुई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम शानदार तरीके से कर रही हैं।
ये स्कूल सप्ताह में छह दिन और रोजाना तीन पालियों में चलाया जाता है। एक पाली तीन घंटे की होती है। यहां बच्चों को बंगला, गणित और सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों के चलते चालन बील के 26 वर्ग किलोमीटर के बाढ़ग्रस्त इलाके में बच्चों की शिक्षा जारी रह पाई है।
नौका वाली स्कूलों में पुस्तकालय और हेल्थ क्लीनिक भी चलाए जा रहे हैं। इस परियोजना के चलते अबतक 22,000 से ज़्यादा छात्र स्नातक हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की संस्था शिधुलाई स्वनिर्वर ने बच्चों की शिक्षा के लिए इस साल यूनेस्को का कन्फ्यूशियस साक्षरता पुरस्कार जीता है।
ये नौका वाले स्कूल स्थानीय लकड़ी से बनी होती हैं। इनमें बेंच, ब्लैकबोर्ड और किताबों की अलमारियां लगी हैं। सौर पैनलों से बिजली के बल्ब और कम्प्यूटर चलते हैं।
एसएसएस के वरिष्ठ प्रबंधक मधुसूदन करमाकर का कहना है कि फ़िलहाल, हमारे 26 नाव स्कूलों में 2,240 छात्र नामांकित हैं। अब तक 22,500 से ज़्यादा छात्र स्नातक हो चुके हैं और भीषण बाढ़ के दौरान ये नावें विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय का भी काम करती हैं।"
इन इलाकों के बच्चों के अभिभावक मोहम्मद रिजवान को अपना नायक मानते हैं। उनका मानना है कि यहां के ज्यादातर उम्रदराज लोगों को कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला लेकिन उनके बच्चे इन नौका स्कूल में अपना भविष्य संवार रहे हैं।
शिधुलाई स्वनिर्वर संस्था प्रबंधन का मानना है कि दो दशक से ज्यादा समय से चलाए जा रहे नौका स्कूल से प्रेरणा पाकर नाइजीरिया, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे देशों में बाढ़ वाले क्षेत्रों में ऐसे नौका वाले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं।
भारत में भी बच्चे और बच्चियों की शिक्षा को लेकर कई लोगों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल के दरवाजे खोले। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। इस स्कूल में सभी जातियों की बच्चियों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिला। तत्काली समाज के मर्दवादी लोगों ने सावित्रीबाई को लड़कियों को शिक्षित नहीं करने देने के लिए तरह-तरह की यातनाएं दी। स्कूल पहुंचने के रास्ते में उनपर कीचड़ और गोबर फेंकते। यही वजह है कि सावित्रीबाई अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं। वह स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ वाली साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनकर लड़कियों को शिक्षित करने में लग जाती थीं।
देश को आजादी हासिल होने से पहले बच्चों की शिक्षा को लेकर गिजुभाई बधेका का प्रयास उल्लेखनीय है। भारत में मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को लागू करवाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर बच्चों की शिक्षा के लिए बाल मंदिर की स्थापना की। उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य भी रचे। बच्चे उनकी बड़ी मूंछों के कारण उन्हें मूंछली मां नाम से बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चों का विकास उनकी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार होना चाहिए।
देश को आजादी मिलने से पहले 1946 में महात्मा गांधी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में लगभग 7 महीने रहे। उन्होंने यह देखा कि इस बस्ती में लोगों के बीच पढ़ाई, लिखाई का माहौल नहीं है। उन्होंने बस्ती के लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजो, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। गांधीजी की कक्षा बस्ती के 30 बच्चों से शुरू हुई। धीरे-धीरे वहां गोल मार्केट, पहाड़गंज, इरविन रोड व आसपास के इलाके के बच्चे भी पढ़ने के लिए पहुंचने लगे। बहुत जल्दी बच्चों की संख्या बढ़कर 75 हो गई।
Updated on:
08 Oct 2025 04:18 pm
Published on:
08 Oct 2025 03:57 pm
बड़ी खबरें
View AllPatrika Special News
ट्रेंडिंग