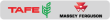आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक दबदबे की दौड़ चल रही है जिससे हम सब परिचित हैं। यह भी एक तथ्य है कि फिलहाल अमेरिका और चीन इस होड़ में सबसे आगे हैं। तीसरा स्थान अभी खाली है और इसे हासिल करने के लिए यूरोप के साथ-साथ भारत भी जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने तीनों प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में हमारी कुछ सीमाएं हैं — एक ऐसा देश होने के नाते जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चलता है और जिसे अपनी बहुत बड़ी आबादी को साथ लेकर चलना एक अनिवार्यता है। लेकिन हमारी कुछ मजबूतियां भी हैं जो अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी में भी सशक्त दावेदार बनाती हैं।
क्या भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक दबदबा कायम कर सकता है — यह सवाल बहुत से भारतीयों के मन में है। हमारे स्टार्टअप इको-सिस्टम, सरकार के फोकस, सेमीकंडक्टरों के क्षेत्र में ठोस पहल, वैश्विक एआई कंपनियों में भारतीयों की मजबूत स्थिति और आईटी में भारत की पारंपरिक बढ़त कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारे लिए उम्मीद पैदा करते हैं।
नंबर वन की दौड़ में पड़ने की बजाय भारत के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि वह दुनिया में एआई इको-सिस्टम का इंजन बने। वह बहुत सारे तरीकों से इस तकनीक के विकास, प्रयोग, मैनेजमेंट की ताकत बने। हालांकि हम भी अपने एआई मॉडल बना रहे हैं, लेकिन उनका प्रधान मकसद अपने आपको विदेशी मॉडलों पर निर्भरता से मुक्त करना है। हम इन मॉडलों को ओपनएआई, गूगल, क्लॉड, मेटा आदि के लोकप्रिय जनरेटिव एआई मॉडलों के मुकाबले किसी किस्म की प्रतिद्वंद्विता में उतारेंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन हां, हम दूसरों की एआई पर इतने निर्भर न हो जाएं कि अगर किसी आड़े वक्त पर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो हम अधर में लटक जाएं — यही हमारी फौरी रणनीति है।
पिछले दिनों अमेरिकी पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' ने लिखा है कि भले ही भारत अमेरिका और चीन जैसी एआई-शक्ति न बने, लेकिन वह 'एक अलग तरह की वैश्विक एआई शक्ति' बन सकता है। इसी नजर में, भारत इन दोनों देशों से अलग रास्ता लेते हुए भी एक विजेता बन सकता है — और वह रास्ता है एआई की मदद से खुद अपना, अपने कारोबार, गवर्नेंस, सेवाओं, शिक्षा, रोजगार, नवाचार आदि का कायाकल्प करने का।
सरकार और उद्योग के प्रयासों के साथ-साथ, इसका एक बड़ा कारण है भारत के लोगों का सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रवैया — अपने तथा अपने देश के भविष्य के प्रति और एआई जैसी नई तकनीकों के प्रति। वास्तव में भारत का आम आदमी, विशेषकर युवा, एआई में मौजूद संभावनाओं के प्रति खुला रवैया दिखा रहा है।
एक विकासशील देश होने के नाते, शायद दुनिया के बहुत से देशों के लिए यह अविश्वसनीय है जो भारत में एआई के पक्ष में चल रहे अंडरकरंट से वाकिफ नहीं हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, वे देश में भीतर ही भीतर चल रही एक अंतरधारा की तरफ इशारा करते हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो भारत एआई से लाभ उठाने वाले देशों में अग्रणी बन सकता है — बिना ओपनएआई तथा गूगल जैसे महाशक्तिशाली एआई मॉडल बनाए।
जहां अमेरिका इस तकनीक को व्यवसाय के अवसर के रूप में और चीन उसे नियंत्रण के साधन के रूप में देख रहा है, वहीं भारत की दृष्टि अलग है। जहां अमेरिका अपनी पूंजी और सिलिकॉन वैली की नवाचार संस्कृति के बल पर इस क्षेत्र में आगे है, वहीं चीन सेंट्रलाइज्ड डेटा और विशाल सरकारी समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत एक 'तीसरी राह' तलाश रहा है — ऐसी शक्ति बनना, जो तकनीकी विकास को केवल बाजार या नियंत्रण का उपकरण न माने, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव और 'सबका साथ' (समावेशन) का साधन बनाए।
आंकड़े बताते हैं कि देश ने इस नवीनतम तकनीक को जिस तरह अपना लिया है, वह उल्लेखनीय है। ओपनएआई का चैटजीपीटी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जबकि एंथ्रोपिक जैसे कई नए एआई प्लेटफॉर्म भी यहीं पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ताजा अध्ययन के अनुसार, दफ्तरों में काम करने वाले 92% भारतीय कर्मचारी रोजाना एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में यही आंकड़ा 64% है। केवल उत्सुकता के आधार पर इतनी बड़ी बढ़त अर्जित नहीं की जा सकती। यह लोगों के मानस में बदलाव की झलक देती है, जो सुखद है तो तर्कसंगत भी — क्योंकि भारत की आबादी में युवा बहुसंख्यक हैं।
युवा, जिन्हें आप डिजिटल नेटिव्स भी कह सकते हैं, तकनीक से डरते नहीं, बल्कि उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वे प्रयोगधर्मी हैं और जोखिम लेने से झिझकते नहीं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक, 70% भारतीय एआई को संभावनाओं से भरपूर मानते हैं। इंफोसिस के सह-संस्थापक और 'आधार' के शिल्पकार नंदन नीलेकणी ने हाल ही कहा कि “भारत को एआई से डर नहीं है, बल्कि उसे अपनाने का विश्वास है, क्योंकि डिजिटल तकनीक ने यहां समावेशन में हाथ बंटाया है।”
भारत को अब जरूरत है तेज रफ्तार से अमल करने की। वर्ष 2027 तक भारत में एआई क्षेत्र में करीब 25 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इस साल देश में एआई का बाजार आठ हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये दोनों तथ्य अपनी जगह हैं, लेकिन सफलता का असली पैमाना लोगों के जीवन में बदलाव का होगा।
अगर बिहार का किसान एआई से मिली सूचनाओं के जरिए 15% अधिक पैदावार पाए, ओडिशा का बच्चा स्थानीय भाषा में ऑनलाइन ट्यूटर से पढ़कर परीक्षा पास करे, और राजस्थान की महिला समय पर एआई-आधारित स्वास्थ्य जांच करवाकर संभावित बीमारी को टाल सके — तो वही असली कायाकल्प है।
तकनीक की सफलता तभी है जब वह जिंदगियां बदले, न कि केवल मुनाफा बढ़ाए।
Published on:
15 Oct 2025 03:22 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग