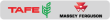भारत ने मई 2025 में 110 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। यह केवल तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत ने विकास और पर्यावरण को एक साथ लेकर चलने वाली नीति को अपनाया है। जहां 2014 में यह आंकड़ा केवल 2.6 गीगावाट था, आज भारत दुनिया में चीन (500 गीगावाट) और अमरीका (160 गीगावाट) के बाद तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। यह केवल सरकारी प्रयासों की नहीं, बल्कि नीति, निवेश और जनभागीदारी की सम्मिलित सफलता है। आज ऊर्जा केवल बिजली पैदा करने का साधन नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का प्रतीक बन चुकी है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 30 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब दूर का सपना नहीं, बल्कि निकटतम यथार्थ है। इसे 'ऊर्जा स्वराज' की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा सकता है, जिसमें उपभोक्ता स्वयं ऊर्जा उत्पादक भी बनता है। इस उपलब्धि के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं रही हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर पार्क योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ), प्रधानमंत्री कुसुम योजना और रूफटॉप सब्सिडी योजना- ये सभी योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर दिखी हैं। पीएम-कुसुम के माध्यम से लाखों किसानों को सौर पंप मिले, जिससे सिंचाई लागत घटी और डीजल पर निर्भरता कम हुई। पीएलआइ के तहत देश में सौर उपकरण निर्माण को बल मिला और रोजगार सृजन को गति मिली। इन योजनाओं ने सिर्फ बिजली नहीं दी, बल्कि रोजगार, जलवायु नीति और कृषि सुधार के अवसर भी दिए। केवल स्थापित क्षमता ही सफलता का मानदंड नहीं है। एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2025 के अनुसार, 2024 में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के मामले में भारत 134 टेरावॉट-घंटे (टीडब्ल्यूएच.) के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन 834 टीडब्ल्यूएच और अमरीका 303 टीडब्ल्यूएच के साथ अग्रणी रहे। जापान (102 टीडब्ल्यूएच) और ब्राजील (75 टीडब्ल्यूएच) भी उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। यह अंतर इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत को अब क्षमता स्थापना से आगे बढ़कर, उत्पादन दक्षता और उपभोग एकीकरण की दिशा में ठोस कार्य करना होगा। जहां जर्मनी और जापान जैसे देश नागरिक सहभागिता आधारित मॉडल पर काम कर रहे हैं, भारत ने नीति, समाज और निजी क्षेत्र- तीनों को साथ लेकर चलने वाला मॉडल विकसित किया है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों और खेतों तक पहुंची है। भारत का अगला लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अब तक की प्रगति को देखकर यह यथार्थ प्रतीत होता है। इसके लिए प्रति वर्ष 25-30 गीगावाट की वृद्धि, ग्रिड स्थिरता, बैटरी भंडारण तकनीकों का विस्तार और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सौर क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रिड समाकलन (ग्रिड इंटीग्रेशन)। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ा है, ग्रिड की स्थिरता एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है । दूसरी समस्या है भूमि अधिग्रहण, खासकर जब कृषि भूमि पर सौर पार्क स्थापित किए जाते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है सौर कचरे का प्रबंधन। 2030 तक भारत में लगभग 20 लाख टन सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है, लेकिन अब तक इसकी रीसाइक्लिंग हेतु कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इन चुनौतियों के समाधान भी संभव हैं- ग्रिड स्थिरता के लिए बैटरी स्टोरेज और माइक्रो-ग्रिड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सौर कचरे के पुन: उपयोग हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) को लागू किया जा सकता है। भूमि उपयोग को लेकर स्थानीय समुदायों को आर्थिक भागीदारी और निर्णय में स्थान मिलना चाहिए। भारत की यह सौर ऊर्जा यात्रा केवल तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, नीति दक्षता और जलवायु प्रतिबद्धता की सम्मिलित सफलता है। अब समय है कि हम सौर शक्ति को केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे एक व्यापक विचार और सामूहिक संकल्प के रूप में देखें। भारत की यह यात्रा विश्व को यह संदेश देती है- 'हम केवल सूरज की किरणें नहीं पकड़ रहे, हम अपना भविष्य गढ़ रहे हैं।'
Published on:
22 Jul 2025 08:22 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग