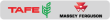फोटो: पत्रिका
संस्कृत एक भाषा है—शब्दों का संग्रह रूप है। माया है। सम-कृत यानी कि ब्रह्म का किया हुआ। ब्रह्म के विस्तार में कारक है। सरस्वती है—आग्नेय है। ब्रह्म ने (सोम) अपने विस्तार के लिए ही माया को पैदा किया था क्योंकि विस्तार ही अग्नि का धर्म है। अव्यय पुरुष की कामना से तपन-स्वेदन हुआ। प्राणों का तपन ही अक्षर सृष्टि है। यही आगे चलकर शब्द रूप तन्मात्रा बनता है।
परमेष्ठी मण्डल से सृष्टि का आंरभ होता है। यहां भृगु-अंगिरा प्राणों से सोम और अग्नि दो धाराएं निकलती हैं। एक पदार्थ या लक्ष्मी की धारा है, दूसरी ऊर्जा रूप सरस्वती की धारा है। यही शब्द तन्मात्रा का रूप लेती है। स्फोट-स्वर-व्यंजन रूप में शब्द ब्रह्म की सृष्टि उसी प्रकार आगे बढ़ती है, जिस प्रकार परात्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर रूप में अर्थ ब्रह्म की सृष्टि स्थूल रूप लेती है। यह शब्द सृष्टि ही संस्कृत है। सृष्टि विस्तार के सिद्धान्तों पर आधारित है।
भाषा कोई भी हो, सम्प्रेषण का माध्यम होती है। किन्तु संस्कृत शायद एकमात्र भाषा है, जो अपने आप में विषय है। संस्कृत सरस्वती रूप में अक्षर प्राणों का धरातल है। जबकि लक्ष्मी जड़ रूप क्षर सृष्टि है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही वाक् हैं। सरस्वती परा वाक् है, लक्ष्मी अपरा वाक् है। लक्ष्मी की प्रतिष्ठा सरस्वती ही है। कृष्ण गीता के सातवें अध्याय में कहते हैं कि मेरी अष्टधा अपरा प्रकृति है एवं दूसरी परा प्रकृति- चेतना रूप है। यही लक्ष्मी एवं सरस्वती हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान मैटर और एनर्जी या पदार्थ और ऊर्जा कहता है। दोनों अविनाभूत हैं।
सरस्वती प्राण रूपा है—अदृश्य है, परोक्ष है, सूक्ष्म है। लक्ष्मी जड़ है। शरीर-मन-बुद्धि भी जड़ हैं। तीनों आत्मा के साधन हैं। शरीर 'मां’ है, पंचभूतों (महाभूत) से बना है। मां का शरीर ही शिशु का अन्न रूप पदार्थ है, जिसकी चिति से गर्भ में शिशु की देह का निर्माण होता है। पृथ्वी-अन्न-महाभूत सभी तो लक्ष्मी के पर्याय हैं। स्त्री वस्तुत: लक्ष्मी है, सौम्या है, ऋत रूप है। परमेष्ठी लोक की लक्ष्मी ही स्थूल रूप होकर पृथ्वी पर अवतरित होती है। स्त्री ही सूक्ष्म प्राण रूपा सरस्वती भी है। हम जीवात्मा रूप चेतन तत्त्व हैं। कर्म के अनुसार वस्त्र रूपी देह बदलते रहते हैं। किन्तु शरीर के भीतर रहने वाला जीवात्मा नष्ट नहीं होता—
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।। (गीता 2.22)
लक्ष्मी पदार्थ रूप है, नष्ट होती जाती है। क्षरण ही इसका पर्याय है। जबकि सरस्वती अर्थात् शब्द आकाश का गुण है। आकाश से ही शेष महाभूत उत्पन्न होते हैं। अत: शब्द-ध्वनि के प्रवाह को अन्य महाभूत रोक नहीं सकते। जैसे प्रकाश को बाधित किया जाता है। जहां शब्द है वहां ध्वनि भी है। ध्वनि से ही पृथ्वी (पांचवा महाभूत) रूपी देह का मातृगर्भ में निर्माण होता है। चूंकि देह का निर्माण भी मातृ देह से होता है, अत: स्वयं देह ही माता है, लक्ष्मी है। जीवात्मा प्राण रूप है, ध्वनि की भांति ही सूक्ष्म, अदृश्य है। अत: ध्वनि-आग्नेय प्राण- के माध्यम से ही मातृगर्भ में जीवात्मा को संस्कारित किया जाता है। ध्वनि-वाक् की चार अवस्थाएं होती हैं—परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी—
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुब्र्राह्मणा ये मनीषिण: ।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ (ऋग्वेद 1.164.45)
एक ही नादात्मक वाणी मूलाधार से उदित होकर परा कहलाती है। नाद के सूक्ष्म एवं अरूप होने के कारण योगियों द्वारा देखने योग्य होने से वही वाणी पश्यन्ती कहलाती है। पश्यन्ती ही बुद्धिगत होने पर सूक्ष्म प्राणी जगत् में अनुभूत होकर मध्यमा कहलाती है। मध्यमा ही मुख में स्थित होकर तालु एवं ओष्ठ आदि की क्रिया से मुख से बाहर निकलती है तब उसे वैखरी कहते है। अत: वाक् का स्थूल रूप वैखरी है।
शरीर की तरह ही शब्द भी क्रियात्मक हैं। वैखरी में मन के भावों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मन में उठने वाली इच्छाओं की अभिव्यक्ति वाक् से होती है। मन और वाक् साथ रहते हैं। अत: जो विषय मन के पार होते हैं, वहां शब्दों की पहुंच नहीं है। यही वैखरी की सीमा बन जाती है। मध्यमा भी छूट जाती है। पश्यन्ती का क्षेत्र शुरू हो जाता है। चूंकि वैखरी के भीतर परा, पश्यन्ती और मध्यमा रहती हैं और इनके साथ-साथ भाव भूमि की शक्ति, गति और दिशा होती है, अत: स्पन्दनों का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जिस प्रकार माया ब्रह्म को गर्भ में लेकर शरीर रूप धारण करती है तथा शरीर अपने आप में जड़ होते हुए भी चैतन्य प्रतीत होता है, इसी तरह वैखरी के गर्भ में परा वाक् को जानना चाहिए। ध्वनि का भावनात्मक-दृश्यात्मक मौन ही पश्यन्ति रूप में जीवात्मा को मानव स्वरूप में परिणत करता है। मां जानती है कि जीवात्मा किस देह को छोड़कर आया है। इसे मानव रूप देना है। मां की दिव्यता भाषा के माध्यम से एवं भावभूमि से ही प्रकट होती है।
जिस प्रकार विश्व (पदार्थ) भाव अर्थवाक् या अर्थब्रह्म है, वैसे ही शब्द वाक्- अंगिरा धारा या सरस्वती प्रधान है। सूर्य सरस्वती मण्डल है, पृथ्वी लक्ष्मी मण्डल है। सूर्य ही जगत का आत्मा है—सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च…। दोनों ही वाक् रूप एक ही साथ रहते हुए, एक ही सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। मां को सिद्धान्त भले ही ज्ञात न हो, मातृ भाषा के आधार पर (प्रत्येक योनि में) भाव रूप शब्द का उपयोग करती है। देह और जीवात्मा एक ही सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।
कृष्ण कहते हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूं। 'अ' से ही सम्पूर्ण वर्णमाला उत्पन्न होती है। शब्द भी इसी वाक् का रूप है। संस्कृत शब्द भी है, अक्षर भी है, अत: सृष्टि के नियमों पर ही कार्य करती है। जिस प्रकार अर्थ सृष्टि में विकारक्षर, पंचजन, पुरंजन, जाति, गोत्र आदि का विकास होता है, उसी क्रम में 'अ' रूप स्वर से ही 288 प्रकार का उच्चारण किया जाता है। अ, इ, उ, ऋ, लृ रूप पंच स्वरों से सम्पूर्ण संस्कृत भाषा का विकास होता है। क्या संस्कृत भाषा को सम (ब्रह्म) और कृत (कृति) रूप में विश्व का मानचित्र (सिद्धान्तों का) नहीं कहा जा सकता?
पंचपर्वा विश्व में यह वाक् सर्वत्र व्याप्त है। स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी की वाक् को क्रमश: गौरी, आम्भृणी, बृहती, सुब्रह्मण्या और अनुष्टुप् वाक् कहा जाता है। हमारी वर्णमाला अनुष्टुप् वाक् है। इसी से भाषा व्यवहार चलता है। वर्णवाक् के गर्भ में स्वरात्मिका वाक् रहती है। वह बृहती है। इसके गर्भ में सुब्रह्मण्या वाक् तथा इसके भी गर्भ में सर्वाधार बनती हुई आम्भृणी वाक् है।
अ-इ-उ-ऋ-लृ (स्वर) का विकास सूर्य से होता है। क-च-ट-त-प (वर्ण) का विकास पृथ्वी से होता है। स्वरों के आधार के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरवाक्-बृहती वाक् ही व्यंजन वाक्- अनुष्टुप वाक् की प्रतिष्ठा है। जो कुछ शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, अथवा कान में सुनाई देते हैं, वे सभी हमारे शरीर तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर मंत्रों से बना है। भक्ति के स्पन्दन रक्तशोधक का कार्य करते हैं। शरीर को रोगों से मुक्त रखते हैं। अप शब्द सुनना-बोलना रोगकारक है।
'अग्नि-सोमात्मकं जगत्’ के अनुसार सभी पदार्थ अग्नि-सोम से उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार स्पर्श (सोम) और उष्मा (अग्नि) से ही सम्पूर्ण वर्णाक्षरों का स्वरूप बनता है। दोनों ही धाराएं समान रूप से साथ चलती हैं। यही कारण है कि शब्द से प्रार्थना-पूजा-यज्ञ-अनुष्ठान का महत्व स्पष्ट हो जाता है। सरस्वती के आधार पर ही लक्ष्मी प्रतिष्ठित रहती है। वाग्देवी सरस्वती मां है, अर्थदेवी लक्ष्मी भी मां है। इन दोनों की धारक-स्त्री- भी मां है। स्त्री की दिव्यता शेष दोनों से ऊपर है। संस्कृत मां है- भाषा ही नहीं जीवन निर्मात्री है।
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Published on:
27 Sept 2025 08:16 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग