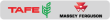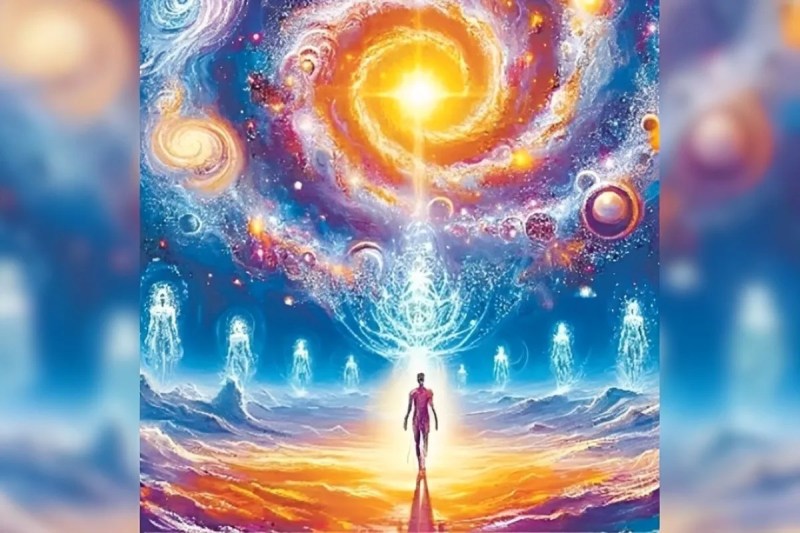
फोटो: पत्रिका
आनीदवातं स्वधया तदेकम्... नासदीय सूक्त के अनुसार ब्रह्म, सृष्टि के आरम्भ में अकेला था, निराकार था। घोर अन्धकार से घिरा हुआ। प्रलय के उस सलिल सागर में स्पन्दित तो था ही, निराकार होने से एक ओर अनन्त था किन्तु उसकी स्वरूप व्याख्या कर पाना असम्भव भी था। ब्रह्म की यह अवस्था अनुपाख्य, अनिर्वचनीय, निर्विशेष आदि नामों से जानी जाती है। यही उसके अहंकार की मूल कहानी है। उसने कामना की—एकोऽहं बहुस्याम्। यह कामना उसके मन के केन्द्र को स्पन्दित कर रही थी। मन में नई ऊर्जाओं का संचार शुरू हुआ। उसे लगा उसके भीतर कोई शक्ति उद्बुद्ध हो रही है। शायद यह उसके लिए आल्हाद का बड़ा क्षण था। उसको लगा कि अब मेरी पहचान हो सकती है। मेरी शक्तियों का प्राकट्य संभव है। पर उसके पहले उसे एक आकार में आने की अनिवार्यता थी। वह तो ऋत सोम ही था। सोम सदा नीचे गिरता है। नीचे आते-आते उसमें उष्णता आ जाती है। मातरिश्वा वायु ने इसी उष्णता से उसका परिचय कराया और दोनों एक हो गए। यह दाम्पत्य भाव ही परात्पर रूप में आगे बढ़ा। आगे की सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरू हुआ।
ब्रह्म स्वयं कुछ करता नहीं। कामना ही उसका पहला और अन्तिम कर्तृत्व था। कामना की प्रेरणा से जो ग्रन्थिबन्धन हुआ वही बिन्दु भाव में ब्रह्म की पहली आकृति बना। ब्रह्म का चूंकि क्षरण नहीं होता अत: इस बिन्दु को अव्यय के नाम से जाना गया। इस बिन्दु में ब्रह्म के सभी गुण समाहित रहते हैं। गीता में कृष्ण ने इसी बिन्दु रूप अव्यय को अपना पर्याय कहा है—मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।। (गीता 7.25) मैं ही अजन्मा अव्यय हूं।
अव्यय को पुरुष कहा जाता है। ‘पुरे वसति इति पुरुष:’ पुर अर्थात् शरीर में जो वास करता है वह पुरुष है। इस पुर के भीतर ही वेदत्रयी कार्य करती है। यजु: को ही पुरुष की संज्ञा दी गई है। साम पुरुष की परिधि है। यही परिधि माया है। जो पुरुष को आवरित करती है। ऋक् केन्द्र है। जिसे श्वोवसीयस मन कहा जाता है। अव्यय पुरुष के सभी कर्म माया के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। मन में माया की कामना ही आनन्द और विज्ञान का स्वरूप निर्मित करती है जो मुक्ति साक्षी कहलाती है। वही माया प्राण और वाक् रूप में अव्यय को सृष्टि की ओर मुखरित करती है। माया ही ब्रह्म के स्वरूपों की अभिव्यक्ति है।
स्थूल जीवन में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री के मध्य दाम्पत्य भाव की एक परम्परा निर्मित की गई है। दो शरीर तो क्षरणशील हैं किन्तु ये शरीर जीवात्मा के कर्मफल भोगने के हेतु बनते हैं। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है। सूक्ष्म शरीर सदा कारण शरीर के साथ ही एकाकार रहता है और देह छोड़ने के बाद भी दोनों शरीर साथ ही रहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कारण शरीर में जो माया की कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं- प्रारब्ध के कारण- वे ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर में कार्यरत दिखाई पड़ती हैं।
सृष्टि रचना में तैंतीस देवता हैं और निन्यानवे असुर हैं। ये सभी माया की ही अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक जीवात्मा में देव और असुर प्राण अपना-अपना कर्म करते रहते हैं। जहां एक ओर मां को जननी रूप में देखते हैं वहीं उसी मां को सन्तान की जीवहन्ता के रूप में भी देख रहे हैं। माया का रूप ब्रह्म के लिए न्योछावर भी है। आज हम देखते हैं कि अनेक षड़यंत्रों के द्वारा स्त्री अपने पति की हत्या में भी हिचक महसूस नहीं करती। माया स्वभाव से भोग्या है किन्तु शक्तिमान की सम्पूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री होने से वह स्वामिनी भी है।
ब्रह्म का विस्तार माया का पहला संकल्प है। कर्मफल के अनुसार ब्रह्म को विभिन्न योनियों में स्थानान्तरित करना भी उसी के कर्म का एक हिस्सा बनता है। जब तक माया और अक्षर प्राण संयुक्त रहते हैं तब तक किसी प्रकार के क्षरण की संभावना नहीं है। हृदय के सभी प्राण अव्यय की शक्तियों से आप्लावित रहते हैं। किन्तु जब स्थूल और सूक्ष्म का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है तब शरीर मात्र- चाहे पुरुष हो या स्त्री- पदार्थ रूप रह जाता है। निश्चेतन हो जाता है। अत: स्वत: ही भोग की वस्तु बन जाता है। यहां माया नहीं है। उनका सम्पर्क कट चुका होता है। वे पशु योनियों की तरह विचरण करते रहते हैं। इस कारण जीवात्मा पुन: ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो पाता।
यही कारण है कि भारतीय मनीषा ने जो जीवन तंत्र विकसित किया उसका लक्ष्य मोक्ष ही रहा ताकि जीवात्मा कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो। माया में ब्रह्म का अंश नहीं होता, वह ब्रह्म की शक्ति के रूप में ब्रह्म के निमित्त कार्य करती है। स्त्री रूप में भी वह अपने ब्रह्मांश को तलाश लेती है। समय के साथ उस ब्रह्मांश को अपने शरीर में खींच लाती है। यही उसका सबसे बड़ा आत्मसम्मान का कर्म है कि ब्रह्म आज उसके शरीर में बन्द है। वह तब तक बन्द रहेगा जब तक कि उसका नया शरीर (योनि के अनुरूप) तैयार नहीं हो जाता। ब्रह्म के लिए आकृति का निर्माण हो रहा है। पुन: उसके भविष्य के अनुरूप उसकी प्रकृति का परिष्कार अथवा संस्कार हो रहा है।
यह पूरा काल माया के उत्तरदायित्व के बोध का काल है। माया के कर्म ही उसकी निपुणता, निर्माण कला एवं ब्रह्म के सुरक्षा कवचों के निर्माण की दक्षता प्रकट करते हैं। इस देह को मनुष्य रूप में सौ साल जीना है। इस हेतु स्त्री रूपी माया दस महीने तक प्रतिक्षण प्रत्येक चिति को अपने शरीर के ताप में निरन्तर पकाती रहती है। जीव को ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित करके समाज को सौंपती है। ब्रह्म का विस्तार करना ही माया को उत्पन्न करने का मूल उद्देश्य है। अब जो सन्तान होगी वह कह सकती है—अहं ब्रह्मास्मि।
निर्मित शरीर में ब्रह्म बैठा है। माया सुप्त है। सही अर्थों में तो माया ब्रह्म की शक्ति तो है किन्तु स्वरूप में वह कहीं संगिनी के रूप में दिखाई नहीं पड़ती। ब्रह्म के स्वरूप से जुड़ी हुई नहीं है। स्त्री को भी हम देखें तो जिस घर में वह आ रही है उसके साथ ब्रह्म नहीं आ रहा, जबकि वह माया बनने को अग्रसर है। उसको पता है कि मुझे अपने पुरुष के पौरुष रूप ब्रह्म का विस्तार करना है। यही उसका मूल लक्ष्य भी है। उसका ध्यान केवल आत्मिक धरातल से जुड़ा रहता है। आहुत होने आई अग्नि में और समाहित हो गई। उसका अपना अस्तित्व यहां से आगे नहीं है। आगे उसे केवल ब्रह्म के विवर्त के लिए कर्म करना है।
वह तो ऐसा बीज बन गई जो धरती में समा गया। उसे पेड़ का निर्माण करना है लेकिन पेड़ का निर्माण उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है बीज के प्राणों का पेड़ में निरन्तर प्रवाह सुरक्षित करना। ताकि वह ब्रह्मांश पुन: पेड़ के फल में प्रवेश कर सके। उसके साथ पूर्वजों के अंश भी बने रहें। वह स्वयं धरती के भीतर ही सिमट कर रह जाती है। केवल प्राण रूप बहती है देह में, ब्रह्म के साथ-साथ। ताकि ब्रह्मांश का स्थानांतरण नए फल में संरक्षित होकर पहुंच सके। यही उसका मुख्य आवरण है। उसके आगे के आवरण योनि के अनुरूप क्षर प्रकृति के द्वारा जुड़ते जाएंगे। किन्तु सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा का वर्ण, अहंकृति, प्रकृति, आकृति और प्रारब्ध कर्मों का विवरण साथ ही रहता है। जहां जीवात्मा के पास पुन: लौटने की योनि उपलब्ध है वहां माया कर्म श्रेणी में उन साधनों की उपलब्धता भी निश्चित करने में सहायक होती है। जीवात्मा और ब्रह्म के मध्य जो आवरण हैं उन आवरणों से बाहर निकल कर स्वयं माया के आवरण से मुक्त होने की क्षमता भी उन पुण्यात्माओं को उपलब्ध कराती है जो अपनी योग्यता प्राप्त कर चुके होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परन्तु जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं—
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। (गीता 7.14)
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com

Published on:
18 Oct 2025 10:21 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग