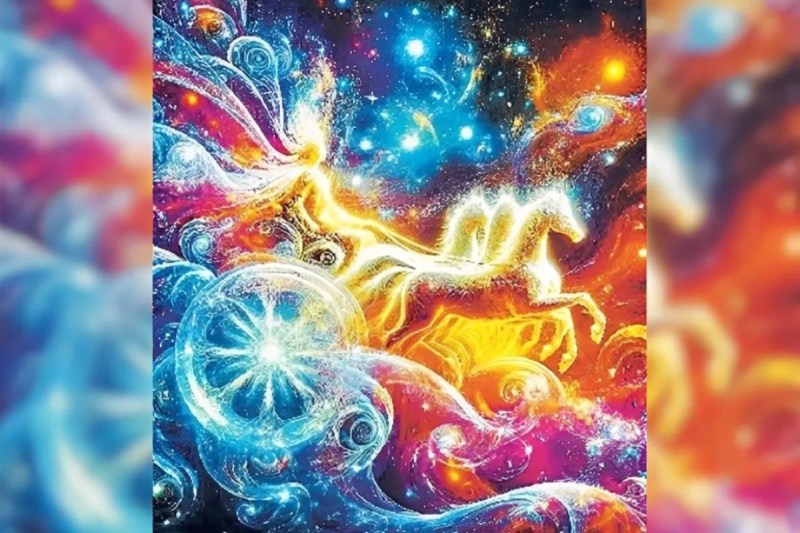
फोटो: पत्रिका
माया ब्रह्म की यात्रा को 84 लाख योनियों में नियोजित करती है। मूल में तो ब्रह्म की भांति माया भी कुछ करती नहीं है। माया कामना है। कामना में गति-कर्म नहीं रहते। होता सब उसके नाम से ही है। माया का कार्य ब्रह्म की व्यवस्था तक ही सीमित रहता है। शेष कार्य आवरणों के हैं, पूर्व कर्मों की इच्छा से जुड़े हैं। इनका कारण-कार्य भाव परा-अपरा प्रकृति करती हैं। इसी माया के द्वारा ईश्वर अपना संचालन बनाए रखता है-
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। (गीता 18.61)
प्रत्येक शरीररूपी यन्त्र में आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार, अपनी माया से, भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है।
निर्माण के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के लिए मन में कामना उठना पहली आवश्यकता है। यह कामना ही माया है। कामना का आश्रय मन है। मन की चंचलता ही कामना का स्वरूप तय करती है। इसके अतिरिक्त भी कामना उदय होती है पूर्व कर्मों के योग से। इसकी पूर्ति को तो टाला ही नहीं जा सकता। अन्त समय में मन को बांधने वाली कामना ही नई योनि के लिए जीवात्मा को प्रेरित करती है। कृष्ण कहते हैं कि भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाल में योगबल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है-
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव।
भु्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।। (गीता 8.10)
गीता में ही कृष्ण अन्यत्र कहते हैं-
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।। (गीता 13.22)
अर्थात् प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी-बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह प्रकृति क्या है इसका भी स्पष्टीकरण कर दिया-
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। (गीता 7.14)
ब्रह्म सृष्टि का मूल तत्त्व है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म ऋत भाव में था, अकेला था। सोम रूप में जल समुद्र में व्याप्त था। शीतलता थी, संकुचन रूप था। मातरिश्वा वायु के कारण जल में बुद्बुद् पैदा हुआ। आकाश स्थिति रूप तथा वायु गत्यात्मक होता है।
बुद्बुद् का केन्द्र सत्य रूप (अव्यय) कहलाया। केन्द्र और परिधि के मध्य यजु: गत्यात्मक पुरुष है। एक ओर अव्यय का निर्माण है, तो दूसरी ओर, हृदय रूप अक्षर प्राणों का निर्माण है। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि व सोम अक्षर प्राण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र को क्रमश: स्थिति, आगति व गति कहते हैं। पिण्ड भाव ही सत्य है। पिण्ड में से निरन्तर क्षरण होता रहता है, उस क्षतिपूर्ति हेतु उसमें सोम की आपूर्ति भी निरन्तर होती रहती है। अभिप्राय है कि निर्माण व ध्वंस दोनों एक ही बिंदु पर अवस्थित हैं। यही अक्षर प्राणों का कार्यक्षेत्र है, जो प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान हैं। सूर्य इस जगत में व्यक्त सृष्टि है। सूर्य में अव्यय, अक्षर, क्षर की पांचों कलाओं के साथ परात्पर की अद्र्धमात्रा भी रहती है। सृष्टि का प्रथम षोडशी पुरुष होने से यही चराचर में आत्म भाव रूप में प्रतिष्ठित रहता है।
ऋग्वेद के दशम मण्डल के 177वें सूक्त में वर्णन मिलता है कि परब्रह्म को तीन गुणों वाली माया से जानते हैं। जिस प्रकार सूर्य को हृदय में नियंत्रित मन- हिरण्यगर्भ- से जानते हैं। सूर्य मण्डल के केन्द्र में जो पुरुष है, वही परब्रह्म है। कवि और विद्वान रश्मियों की नहीं, सूर्य मण्डल की उपासना करते हैं। सूर्य की तरह परब्रह्म का जीवात्मा है, उसे भी विद्वान लोग अन्तर्मुखी मन से ही जानते हैं। तब परब्रह्म और जीवात्मा के रूप में समानता देख सकते हैं। अर्थात् हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म की मन से तुलना करते हैं। जिस प्रकार बाह्य रूपा मिथ्या भाव रश्मियों के स्थान पर विद्वान उपासक सूर्य पर ही ध्यान केन्द्रित रखते हैं।
परमात्मा ने विश्व की रचना की। 'क्या-क्या रचना करनी है’ इसी कामना रूप मन से सृष्टि की। प्रारम्भ का सारा निर्माण वेद के शब्दों से ही किया गया। हिरण्यगर्भ ने उस वाणी का प्रथम उच्चारण किया। इस वाणी की ब्रह्म के स्थान में गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। शरीर में हृदय ही वाणी का गुप्त स्थान है। सूर्य प्रात: हमें (हर प्राणी को) लक्ष्य करके आता है। सायं वही सूर्य पराङ्मुख होकर चला जाता है। दिन में रक्षा करने वाला संध्या में विदा हो जाता है। रक्षा भाव से उदय अस्त होना ही सूर्य की भूमिका है। इसी प्रकार प्राण भी शरीर के रक्षक, अविनाशी, सम्मुख एवं पराङ्मुख होते जाते हैं। सूर्य आकाश मार्ग से विचरण करता है, प्राण नाड़ी मार्गों से विचरण करते हैं।
जीवात्मा को केन्द्रस्थ मन स्वरूप के ब्रह्म से तारतम्य द्वारा ही जाना जा सकता है। अव्यय का यह मन ही श्वोवसीयस मन है। अन्य सभी मन के भी मिथ्या रूप ही माने गए हैं- नश्वर हैं। अव्यय की वेदत्रयी- ऋक्-यजु:-साम ही वाणी का रूप है। सूर्य इस वाणी को बुद्धि से धारण करते हैं।सूर्य भी तीनों वेदों के साथ भ्रमण करते हैं। प्रात: ऋचाओं के साथ, दोपहर में यजुर्वेद के साथ तथा सायंकाल में सामवेद के साथ। शरीर में विद्यमान प्राणवायु ही वाणी को प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार यह वाणी मन रूप सूर्य में रक्षित रहती है, उसी प्रकार शरीर के मध्य स्थित मन में रक्षित रहती है। परमात्मा सृष्टि को आरंभ में मन से धारण करते हैं।
जीवात्मा में भी बीजरूप से सारे शब्द रहते हैं। गर्भावस्था में ही गंधर्व उसके मन में शब्द बीज को बो देते हैं। अत: वाणी की शक्ति असीम है। सूर्य पिता होने से शब्दब्रह्म रूप में कार्य करता है। माता अर्थब्रह्म है, धरती रूपा है। माता के भीतर ही माया का अंश भी रहता है। जहां-जहां ब्रह्म है, वहीं माया भी है। दोनों तत्त्व सुसूक्ष्म होने से जाने नहीं जाते। अनुभूति में तो आते ही हैं। नहीं तो इनके अस्तित्व का महत्व ही खो जाएगा। माया को समझने के लिए ब्रह्म के यात्रा मार्ग पर साथ चलकर समझना होगा। ब्रह्म ने माया को पैदा किया अपने विस्तार के लिए। वह अन्यत्र क्यों मिलेगी। मायाबल रूप में ब्रह्म को विस्तार देती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। अद्र्धनारीश्वर की भांति ब्रह्म का अंश बनकर ही रहती है।
सूर्य के आगे क्षर सृष्टि उत्पन्न होती है। चौरासी लाख योनियों का बीज यहीं से चलता है। माया यहां प्रकृति रूप में रहती है। स्थूल सृष्टि तक पहुंचते-पहुंचते ब्रह्म के ऊपर माया, महामाया, अहंकृति, आकृति, प्रकृति आदि अनेक आवरण चढ़ जाते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि में ब्रह्म और माया अनुस्यूत रहकर यात्रा करते हैं। इसलिए सृष्टि का प्रत्येक प्राणी अद्र्धनारीश्वर है। ब्रह्म आवरित होता है। माया आवरित करती है। ब्रह्म और माया का, प्रकृति और पुरुष का यही मूल सूत्र है। पुरुष जैसे-जैसे आवरणों को समझता जाता है। उनसे मुक्त होता जाता है। माया के बंधन खुलते जाते हैं। माया ही बन्धन और मुक्ति का हेतु है। अन्त में माया के ब्रह्म में लीन होने से प्रकृति का खेल और ब्रह्म की लीला समाप्त हो जाती है।
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Published on:
01 Nov 2025 07:59 am

बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग
