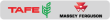फोटो: पत्रिका
ब्रह्म और माया का प्रथम अवतार हुआ अव्यय पुरुष। उसका हृदय हुआ अक्षर पुरुष। अव्यय वेदत्रयी रूप-ऋक्-यजु:-साम है। अक्षर रूप हृदय में प्राणरूप ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र रहते हैं। इन तीनों को युगल रूप में माया ने ही पैदा किया था। दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है कि त्रिगुणमयी महालक्ष्मी ही सबका आदिकारण है।
इस जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा महामाया, महाकाली, कालरात्रि, दुरत्यया आदि अभिधानों से सुशोभित देवी का रूप धारण किया। सत्वगुण के द्वारा महालक्ष्मी ने सरस्वती महाविद्या, भारती, कामधेनु आदि नामों वाली देवी का रूप धारण किया। रजोगुण रूप उपाधि के द्वारा महालक्ष्मी ने गौरी, श्री, मेधा आदि नामों वाली देवी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी-हिरण्यमयी, विष्णु के साथ गौरी, इन्द्र (शिव) के साथ सरस्वती को क्रमश: महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने उत्पन्न किया। विष्णु-ब्रह्मा-शिव क्रमश: सत्व, रज, तम के स्वामी हैं। माया ने युगल रूप में ब्रह्मा-सरस्वती, विष्णु-लक्ष्मी, शिव-गौरी को संकल्पित करा दिया—
ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम्।
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्।।
(दुर्गा सप्तशती प्राधानिक रहस्य/२६)
ब्रह्मा बाहर (पुरुष रूप) रजोगुणी, उनका भीतर का स्त्रैण भाग तमोगुणी हुआ। सरस्वती बाहर तमोगुणी-भीतर रजोगुणी (वाक्) हुई। स्त्री-पुरुष के भीतरी भाग ही तो दोनों के पूरक बनते हैं। ब्रह्मा जहां माया पुत्र हैं, वहीं सरस्वती शिव की भगिनी है शिव उनके पीहर (पितृगृह) के प्रतिनिधि हैं। विवाह पश्चात् दोनों के आत्मा के गुण बदल जाते हैं। विष्णु सत्वगुणी तो हैं, किन्तु लक्ष्मी रजोगुणी है। कार्य तो विष्णु के लिए रजोगुणी होते हुए भी सत्व रूप ही करेगी। किन्तु विष्णु के सत्व के साथ ही शिव का तमस भी जुड़ जाएगा। विष्णु के शुक्र में सत्व के साथ में तम का प्रभाव भी होगा। लक्ष्मी पृथ्वी है—पदार्थ है, आकृति देती है। उसका रज सृष्टि को त्रिगुणी बना देता है। अर्थवाक्, जड़ सम्पदा लक्ष्मी-विष्णु (सोम) की सृष्टि है। ब्रह्मा की रजोगुणी सृष्टि में शब्द वाक् स्पष्ट रहती है। शिव के संहार में काली का तम साथ जुड़ा होता है। शिव श्वेत हैं।
भारतीय विवाह परम्परा पशुओं की भांति शरीरों का मेल नहीं है। यह प्रकृति आधारित भी है और व्यक्ति आधारित भी (सात पीढिय़ों का सूत्र)। इसमें स्त्री-पुरुष के अलावा दोनों पक्षों के पितरों के प्राण भी नई सन्तान में पहुंचते हैं। तब पुरुष शरीर में स्त्रैण भाग पर ससुराल का प्रभाव रहता है। स्त्री शरीर में भी पति के परिवार एवं पूर्वजों का प्रभाव स्पष्ट है। नई विवाह संस्था में स्त्री के परिवार का अंश नई सन्तान तक नहीं पहुंचता। स्त्री के मूल प्राण उसके पिता के पास ही रह जाते हैं। तब सन्तान का आकर्षण दोनों परिवारों में बंट जाता है। स्त्री भी दोनों परिवारों के मध्य जीती है।
विवाह के बाद पुरुष के स्त्रैण भाव का पोषण स्त्री के सोम से होता है। और स्त्री के पौरुष को पुरुष सींचता है। आज नई व्यवस्था में स्त्री-पुरुष दोनों का स्वरूप नहीं बदलता, दोनों अपने-अपने भागों का पोषण जीवनसाथी के अद्र्धांग में नहीं करते हैं। परस्पर विवाह सूत्र की पकड़ ढीली रह जाती है। ऊपर से यदि स्त्री अति बुद्धिमान हुई अथवा अति महत्वाकांक्षी हुई तो दोनों पुरुष रूप लम्बी यात्रा साथ-साथ नहीं कर पाएंगे। आत्मभाव पैदा होना कठिन है। अथवा स्त्री दृढ़ संकल्पवान हो तो लम्बा संघर्ष करके अपना स्थूल स्थान तो सम्मानजनक बना सकती है, किन्तु उसके सात पीढ़ी के अंश सन्तान को प्राप्त नहीं हो सकते।
हमारा दर्शन कर्म-कर्मफल-पुनर्जन्म पर आधारित है। इसका एक ही अर्थ है कि हम जैसा करते हैं, वैसा ही लौटकर हमारे पास आता है। आज चारों ओर जैसा अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा अनाचार फैला हुआ है, उसके कारण भी हम ही हैं। मेरा सुख, मेरा दु:ख, दोनों मेरे कारण ही हैं। समष्टि रूप में समाज का स्वरूप भी मेरे कारण ही बनता है। व्यक्ति से ही समाज बनता है। अत: समाज को भला-बुरा कहते समय स्वयं को प्रश्न कर लेना चाहिए। शिक्षा ने एक प्रकार का अपेक्षा भाव हर व्यक्ति के मन में जगा दिया, किन्तु व्यक्ति को उस के लायक नहीं बनाया। सरकार निश्चेष्ट है- उच्च शिक्षा भारतीय मूल्यों की चर्चा ही नहीं करती। शिक्षा में व्यक्ति की चर्चा ही सुनाई नहीं देती। विषय प्रधान होकर रह गई है।
शिक्षा में विषय की प्रवीणता है, व्यक्तित्व का ह्रास है। अध्यात्म के चार अंगों में से शिक्षा दो अंगों का ही पोषण करती है- शरीर और बुद्धि का। शेष दो अंगों की भूमिका अल्पतम रह जाती है—मन और आत्मा की। एक अच्छे व्यक्ति को असंतुलित कर देती है। उच्च शिक्षा-अधिक असंतुलन। यह एक भाग है। दूसरा भाग है—समानता की अवधारणा का, जिसका अर्थ ही शायद स्पष्ट नहीं है। पश्चिम की अंधी नकल मात्र है। पश्चिम में समाज व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति-स्त्री हो या पुरुष, एकल इकाई के रूप में रहता/रहती है। कानून भी एकल को ही सम्बोधित करते हैं। दांपत्य भाव में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपनी निश्चित पहचान है। दोनों का साथ रहना या अलग होना सामान्य जीवन शैली का अंग है। यही कारण है कि वहां लिव-इन सामान्य बात है। संतान न होना भी इसी अवधारणा का परिणाम है।
भारतीय दर्शन में यह स्वच्छन्दाचार कहलाता है। मर्यादा की परिधि ही आकृति का निर्माण करती है। आकृति ही सत्य भाव है। निराकार का स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। पश्चिम की नकल में शिक्षित भारतीय स्त्री भी निराकार जीने को उतावली है। हवा-पानी की तरह। यही जीवन के उजाड़ की शुरुआत है। नकल में व्यक्ति स्वयं को देखना भूल जाता है, सामने वाले पर आंख रहती है। हमको प्रकृति पैदा करती है। प्रकृति की सच्चाई कुछ और ही है।
आधुनिक शिक्षा का बड़ा अभिशाप यह है कि इसमें अधिदेव की शिक्षा नहीं है। भारतीय जीवन पद्धति तीन धरातलों में प्रतिष्ठित है—आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। पश्चिम में भी अधिदेव की शिक्षा नहीं है जो कि प्राणों का क्षेत्र है। हम तो आत्मा को प्राण रूप मानते हैं। सारे देवी-देवता, असुर आदि प्राण सृष्टि के ही अंग हैं। अधिभूत में भौतिक जगत है और अध्यात्म में शरीर संस्था है। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल और कारण शरीर के बीच का सेतु है। इसके अभाव में जीवन स्वतंत्र रूप से दो खण्डों में बंट जाता है। दोनों ही खण्डों में व्यक्ति अलग-अलग जीता है। तब पूर्णता कैसे संभव है।
अधिदेव के अभाव में शरीर पिण्डमात्र रह जाता है, जैसा मेडिकल साइन्स में देखा जा सकता है। इसका प्रभाव आत्मा (कारण शरीर) तक पहुंच ही नहीं पाता। अधिभूत केवल भोग की वस्तु बनकर रह जाता है। अधिदेव रहित जीवन पदार्थ रूप में भोग की वस्तु बन जाता है। संपूर्ण पश्चिम-विकसित देश- इसका प्रमाण है। दुर्भाग्य से हमारे देश की शिक्षा उसी दिशा में ले जा रही है। वैसा ही हमारा विकास होगा। विवाह शरीर मात्र की आवश्यकता बनती जाएगी। जमीन की तरह शरीर भी मुद्रा का रूप लेता जा रहा है। आत्मा सुप्त होने से कचोटता नहीं है। संवेदनहीन जीवन में प्रेम की धड़कनें शान्त होती जा रही है। क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी-स्त्री- ने मानवता का निर्माण बन्द कर दिया है।
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Updated on:
11 Oct 2025 08:43 am
Published on:
11 Oct 2025 08:42 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग