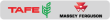अर्थशास्त्र की दुनिया में 2025 का वर्ष इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा घोषित इस वर्ष का सर्विंग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल उन तीन मनीषियों जोएल मोक्यर, फिलिप एघियोन और पीटर हाउइट को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिन्होंने अपने अद्वितीय अनुसंधान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ‘आविष्कार-प्रेरित आर्थिक वृद्धि’ ही आधुनिक विश्व की समृद्धि और प्रगति की आधारशिला है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों के कार्य न केवल आर्थिक सिद्धांतों की नई दिशा तय करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि नवाचार किस प्रकार समाज, संस्कृति और नीतियों के साथ संवाद करते हुए सतत आर्थिक विकास की रूपरेखा निर्मित करता है।
इतिहास साक्षी है कि सभ्यताओं का उत्कर्ष केवल संसाधनों या भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि विचारों की गति और नवाचार की चेतना पर भी उतना ही आधारित रहा है। मोक्यर का शोध इसी तथ्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिपादित करता है। नीदरलैंड में जन्मे और वर्तमान में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी (अमेरिका) में कार्यरत मोक्यर ने अपने अनुसंधान के माध्यम से यह दिखाया कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति का वास्तविक बीज ‘ज्ञान-संस्कृति’ में निहित था। उनके अनुसार यूरोप की प्रगति केवल तकनीकी या पूंजीगत कारणों से नहीं हुई, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा, खुलापन और विचारों के आदान-प्रदान की संस्कृति ने इसे संभव बनाया। 17वीं और 18वीं सदी में जब समाजों ने ‘ज्ञान का संचय’ शुरू किया, जहां प्रयोग, परीक्षण और सत्यापन को प्राथमिकता दी गई, वहीं से मानवता ने निरंतर प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके अनुसार, किसी भी सभ्यता का सतत विकास तभी संभव है जब ‘उपयोगी ज्ञान’ का प्रवाह अबाध रूप से बना रहे। यह ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं, बल्कि व्यावहारिक और सृजनात्मक होना चाहिए — वह ज्ञान जो प्रयोगशालाओं से निकलकर समाज और उद्योग में नई ऊर्जा का संचार करे। मोक्यर का यह दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास की परंपरागत सीमाओं को तोड़ता है और विकास को केवल पूंजी या श्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे विचारों और नवाचार की शक्ति से जोड़ देता है।
दूसरी ओर, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फिलिप एघियोन और कनाडाई अर्थशास्त्री पीटर हाउइट ने ‘शुम्पेटरियन ग्रोथ थ्योरी’ को नए गणितीय और नीतिगत आयाम दिए। उन्होंने यह समझाया कि नवाचार केवल सृजन नहीं, बल्कि विनाश का भी साधन है — एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नई तकनीकें पुरानी को विस्थापित करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था निरंतर गति में बनी रहती है। यह ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ का सिद्धांत है, जिसे जोसेफ शुम्पेटर ने बीसवीं सदी के आरंभ में प्रतिपादित किया था, परंतु एघियोन और हाउइट ने इसे गणितीय मॉडल में ढालकर यह दिखाया कि कैसे यह प्रक्रिया दीर्घकालिक आर्थिक विकास का स्रोत बनती है। उनके मॉडल के अनुसार, जब कोई नया आविष्कार किसी पुराने उत्पाद या तकनीक को प्रतिस्थापित करता है, तो इससे अस्थायी असमानता और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, परंतु दीर्घकाल में यही प्रक्रिया समाज को अधिक उत्पादक, कुशल और उन्नत बनाती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवाचार तभी फलीभूत होता है जब समाज परिवर्तन के प्रति खुला हो, जब नीति-निर्माण पुराने उद्योगों के संरक्षण की बजाय नए विचारों के प्रस्फुटन को प्रोत्साहित करे।
आज विश्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उत्पादकता वृद्धि धीमी पड़ रही है और परंपरागत विकास मॉडल अपनी सीमाएं दिखा रहे हैं। ऐसे में मोक्यर, एघियोन और हाउइट का कार्य भविष्य के लिए प्रकाशस्तंभ की भांति है। यह बताता है कि विकास की वास्तविक शक्ति मानव की नवोन्मेषी क्षमता में निहित है। भारत जैसे देशों के लिए यह विचार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जहां युवा जनसंख्या, डिजिटल प्रगति और उद्यमशीलता की भावना एक साथ नई संभावनाएं खोल रहे हैं। यदि शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करे, उद्योग अनुसंधान में निवेश बढ़ाएं, और सरकार नवाचार के लिए अनुकूल नीतियां बनाए तो भारत आने वाले दशकों में ‘ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था’ की दिशा में अग्रसर हो सकता है।
Published on:
16 Oct 2025 03:46 pm
बड़ी खबरें
View Allसमाचार
ट्रेंडिंग