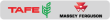बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में सबसे पहले यह समझना होगा कि यहां के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का गणित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आकांक्षाओं, जातिगत स्मृतियों, विश्वास के वादों व राजनीतिक संस्कृतियों के टकराव का अखाड़ा भी है। बिहार में सत्ता को केवल कुर्सी नहीं, बल्कि इतिहास की चोटों और उम्मीदों की मरहम-पट्टी समझा जाता है। यहां की राजनीति में चुनाव नए विमर्शों को जन्म देता है और हर वादा लंबे सामाजिक संघर्ष का प्रतिबिंब होता है।
बिहार का मतदाता अब पहले जैसा भावनात्मक नहीं रहा, मगर भावनाओं से पूरी तरह मुक्त भी नहीं है। वह परिवर्तन चाहता है पर वह परिवर्तन किस आधार पर हो, इस पर उसकी दृष्टि निरंतर परिपक्व हो रही है। बिहार में वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य बहुवर्णी है। एक ओर पुरानी समाजवादी विरासत की याद दिलाने वाले चेहरे हैं, दूसरी ओर विश्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को सामने रखने वाले नेता। एक तरफ जाति की पहचान पर आधारित राजनीति का पुराना संसार है, दूसरी तरफ बदलते युवा वर्ग की आकांक्षाओं का नया संसार।
इन दोनों के बीच एक अदृश्य रस्साकशी चलती रहती है। यहां का मतदाता जानता है कि उसकी जातीय पहचान उससे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी है, फिर भी वह सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार को भी महत्त्व देता है। इसलिए बिहार में चुनावी भाषा दोहरी होती है- एक तरफ ‘पहचान’, दूसरी ओर ‘विश्वास’ और इस दोहरेपन में ही बिहार के लोकतंत्र का चरित्र दिखाई देता है। युवाओं की भूमिका इस चुनावी माहौल में अत्यंत निर्णायक है। बेरोजगारी बिहार का स्थायी संकट रही है और चुनावी प्रचार में रोजगार सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी निराशा दोनों रहा है। युवा वर्ग को आज केवल वादों की सूची नहीं चाहिए, उसे भरोसे की भाषा चाहिए। बिहार का युवा अब यह मानने को तैयार नहीं कि उसके सपने किसी राजनीतिक नारे में सिमट जाएं। वह अवसर चाहता है और यह मौका अपने ही राज्य में तलाशना चाहता है।
इस चुनाव में सामाजिक समीकरण भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने विश्वास के मुद्दे। बिहार की राजनीति बिना जातीय संदर्भ के समझी ही नहीं जा सकती, लेकिन एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है- जाति अब निर्णायक तो है, पर केवल आधार नहीं। जैसे-जैसे शिक्षा और सूचना का प्रसार हुआ है, जातीय भावनाओं का आयाम थोड़ा बदला है। अब मतदाता केवल इस आधार पर वोट नहीं देता कि कौन किस जाति से है, बल्कि यह भी देखता है कि कौन उसकी आकांक्षाओं को समझ रहा है। यह धीमा परंतु महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है, जो बिहार के लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत देता है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीतिक दल इस सामाजिक यथार्थ को पूरी तरह स्वीकारने को तैयार नहीं। वे अब भी जाति के समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उन्हें हर बार एक नए इम्तिहान से गुजरने को मजबूर करती है।
बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में सबसे पहले यह समझना होगा कि यहां के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का गणित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आकांक्षाओं, जातिगत स्मृतियों, विश्वास के वादों व राजनीतिक संस्कृतियों के टकराव का अखाड़ा भी है। बिहार में सत्ता को केवल कुर्सी नहीं, बल्कि इतिहास की चोटों और उम्मीदों की मरहम-पट्टी समझा जाता है। यहां की राजनीति में चुनाव नए विमर्शों को जन्म देता है और हर वादा लंबे सामाजिक संघर्ष का प्रतिबिंब होता है।
बिहार का मतदाता अब पहले जैसा भावनात्मक नहीं रहा, मगर भावनाओं से पूरी तरह मुक्त भी नहीं है। वह परिवर्तन चाहता है पर वह परिवर्तन किस आधार पर हो, इस पर उसकी दृष्टि निरंतर परिपक्व हो रही है। बिहार में वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य बहुवर्णी है। एक ओर पुरानी समाजवादी विरासत की याद दिलाने वाले चेहरे हैं, दूसरी ओर विश्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को सामने रखने वाले नेता। एक तरफ जाति की पहचान पर आधारित राजनीति का पुराना संसार है, दूसरी तरफ बदलते युवा वर्ग की आकांक्षाओं का नया संसार।
इन दोनों के बीच एक अदृश्य रस्साकशी चलती रहती है। यहां का मतदाता जानता है कि उसकी जातीय पहचान उससे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी है, फिर भी वह सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार को भी महत्त्व देता है। इसलिए बिहार में चुनावी भाषा दोहरी होती है- एक तरफ ‘पहचान’, दूसरी ओर ‘विश्वास’ और इस दोहरेपन में ही बिहार के लोकतंत्र का चरित्र दिखाई देता है। युवाओं की भूमिका इस चुनावी माहौल में अत्यंत निर्णायक है। बेरोजगारी बिहार का स्थायी संकट रही है और चुनावी प्रचार में रोजगार सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी निराशा दोनों रहा है। युवा वर्ग को आज केवल वादों की सूची नहीं चाहिए, उसे भरोसे की भाषा चाहिए। बिहार का युवा अब यह मानने को तैयार नहीं कि उसके सपने किसी राजनीतिक नारे में सिमट जाएं। वह अवसर चाहता है और यह मौका अपने ही राज्य में तलाशना चाहता है।
इस चुनाव में सामाजिक समीकरण भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने विश्वास के मुद्दे। बिहार की राजनीति बिना जातीय संदर्भ के समझी ही नहीं जा सकती, लेकिन एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है- जाति अब निर्णायक तो है, पर केवल आधार नहीं। जैसे-जैसे शिक्षा और सूचना का प्रसार हुआ है, जातीय भावनाओं का आयाम थोड़ा बदला है। अब मतदाता केवल इस आधार पर वोट नहीं देता कि कौन किस जाति से है, बल्कि यह भी देखता है कि कौन उसकी आकांक्षाओं को समझ रहा है। यह धीमा परंतु महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है, जो बिहार के लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत देता है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीतिक दल इस सामाजिक यथार्थ को पूरी तरह स्वीकारने को तैयार नहीं। वे अब भी जाति के समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उन्हें हर बार एक नए इम्तिहान से गुजरने को मजबूर करती है।
Published on:
02 Nov 2025 02:52 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग