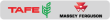यह हर्ष का विषय है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय व एल्सेविएर पब्लिशर की ओर से वर्ष 2024 में जारी शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में भारत के 5300 वैज्ञानिकों ने स्थान बनाया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से नोबेल पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान के लिए किसी का नामांकित न हो पाना बड़ी चुनौती है। कुछ दिन पूर्व ही घोषित नोबेल पुरस्कारों ने इस प्रश्न को पुन: जीवंत कर दिया है कि भारत जैसे विशाल, युवा और प्राचीन ज्ञान परंपरा वाले राष्ट्र से इस प्रतिष्ठित सूची में लोग स्थान क्यों नहीं बना पाते हैं। अब तक भारत से संबंधित लगभग दस व्यक्तित्वों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहां यह रेखांकित करना उचित होगा कि इन सबमें से अधिकांश वैज्ञानिकों ने अपनी महत्वपूर्ण शोध यात्रा व प्रयास भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों व प्रयोगशालाओं में पूर्ण किए, जिससे यह और भी विचारणीय है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रणाली में कहां और किस स्तर पर कमी रह रही है। प्रायः इस विफलता के मूल में हमारे विश्वविद्यालयों में शोध व अनुसंधान के लिए उपयुक्त अवसर व अवसंरचना का अभाव बताया जाता रहा है। केंद्रीय संस्थानों को छोड़ दें तो अन्य राज्य पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं पुरानी हैं, उपकरण पुराने व जर्जर हैं और अनुसंधान के लिए वांछनीय वित्तीय संसाधन सीमित हैं।
यह सर्वकालिक सत्य है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में स्थायित्व और गहराई के लिए दीर्घकालिक निवेश अनिवार्य होता है, जो भारत में प्रायः साल-दर-साल परिवर्तित होने वाले सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहता है। जब तक विश्वविद्यालयों को स्थायी, अनुमाननीय और पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं सुलभ होगा, तब तक दीर्घकालिक मौलिक शोध की संस्कृति विकसित हो पाना कठिन है। इसके अलावा हमारी शिक्षा-पद्धति का स्वरूप भी इसका एक कारण हो सकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा अब भी प्रमुखत: परीक्षा-केन्द्रित और स्मृति-आधारित है। छात्रों को जिज्ञासा, प्रयोग और रचनात्मकता के लिए पर्याप्त अवसर व प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।
सभी नोबेल पुरस्कार विजेता विचारक या वैज्ञानिकों की यात्रा अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि उन सभी ने तथ्यों से परे जाकर प्रयोगों, विफलताओं और नवाचारों से सीखा है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ही ऐसा तो नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को ‘त्रुटि करने की स्वतंत्रता’ बहुत कम है। शिक्षक-छात्र संवाद भी प्रायः एक तरफा ही होता देखा गया है, जिससे प्रश्न पूछने और सोचने की भावना कुंठित होती है, जिससे निसंदेह शोध-मार्गदर्शन और अकादमिक संस्कृति प्रभावित होती है। प्रायः यह पाया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक बाधाएं, धीमी अनुदान प्रक्रिया और परिणामों के लिए त्वरित दबाव दीर्घकालिक अनुसंधान प्रयासों को अवरुद्ध कर देते हैं। यद्यपि इन परिस्थितियों के सुधार के लिए सरकार ने कुछ राष्ट्रीय योजनाएं प्रारंभ की हैं, जो उत्साहवर्धक हैं तथापि उनका त्वरित व उचित क्रियान्वयन ही इन योजनाओं की सफलता की सच्ची कहानी रच सकेगा। प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप के अंतर्गत उच्च प्रतिभाशाली पीएचडी छात्रों को उदार अनुदान दिया जाता है, जिससे वे देश में ही अनुसंधान कर सकें।
इम्प्रिंट और इंस्पायर जैसी योजनाएं विज्ञान और तकनीकी में नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। साथ ही स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कदम युवाओं को अनुसंधान और उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। कुछ समय पूर्व आरंभ की गई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी एक बड़ा कदम है, जो राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सुव्यवस्थित वित्तीय ढांचा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इन सभी योजनाओं में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-संस्कृति को परिवर्तन करने की अपार संभावनाएं हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति देना भी कितना लाभकारी रहेगा, यह देखना भी रोचक होगा। सरकार ने हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस दिशा में अनुमति दी है। यदि प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने केन्द्र खोलते हैं तो यह न केवल वैश्विक मानकों की शिक्षा को देश में लाएगा अपितु अनुसंधान और अकादमिक सहयोग का उचित वातावरण तैयार कर सकता है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, किंतु उस प्रतिभा को सही समय पर पहचानने और पोषित करने की उचित संस्थागत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। देश के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक स्वायत्तता, दीर्घकालिक अनुसंधान वित्तीय सहायता व रचनात्मक स्वतंत्रता वांछनीय है। जब तक विश्वविद्यालयों को प्रयोग और जोखिम उठाने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक वहां से नोबेल पुरस्कार स्तर नामित होने का मौलिक शोध व अनुसंधान होना कठिन होगा। भारत के पास आज भी वह जनसंख्या, ऊर्जा और अकादमिक परंपरा है जो किसी भी राष्ट्र को वैज्ञानिक महाशक्ति बना सकती है।
आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा परीक्षा-केन्द्रितता से निकलकर प्रयोग और नवाचार की संस्कृति में रूपांतरित हो। सरकारी योजनाओं, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सम्मिलित प्रयासों से भारतीय विश्वविद्यालय उस दिशा में बढ़ सकते हैं जहां से वे फिर से विश्व को ज्ञान देने की ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। यदि यह परिवर्तन लागू हुआ तो आने वाले दशकों में भारत से न सिर्फ और नोबेल विजेता निकलने की संभावना है, अपितु विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य में वह मानवीय प्रगति का नेतृत्व भी करेगा।
Published on:
28 Oct 2025 04:01 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग